नक्सलियों का आत्मसमर्पण : हिंसा से संवाद और विकास की दिशा में नया भारत
भारत के जंगलों में बंदूक की जगह संवाद की आवाज़ गूंजने लगी है। आत्मसमर्पण की बढ़ती घटनाएँ बताती हैं कि अब परिवर्तन की राह हिंसा नहीं, विश्वास और विकास से होकर गुजरती है।

भारत के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में नक्सलवाद आधी सदी से अधिक समय से चुनौती बना हुआ है। यह आंदोलन कभी सामाजिक असमानता, भूमि अधिकारों की मांग और आर्थिक अन्याय के विरुद्ध आवाज़ के रूप में उभरा था, लेकिन समय के साथ इसमें वैचारिक दिशा का क्षरण और हिंसक प्रवृत्तियों का विस्तार हुआ। आज जब देश के कई नक्सल प्रभावित जिलों में आत्मसमर्पण की ख़बरें बार-बार सामने आ रही हैं, तो यह केवल हथियार डालने की नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन की कहानी बन चुकी है।
बदलाव की बयार और आँकड़ों की तस्वीर
गृह मंत्रालय के अनुसार 2010 के मुकाबले नक्सल हिंसा की घटनाओं में लगभग 80 प्रतिशत कमी आई है। वर्ष 2024 में जहाँ करीब 1,200 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, वहीं 2025 के पहले नौ महीनों में यह संख्या 1,500 से अधिक पहुँच चुकी है। विशेष रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में आत्मसमर्पण की दर तेज़ी से बढ़ी है। केवल बस्तर क्षेत्र में पिछले वर्ष 400 से अधिक सक्रिय सदस्य और समर्थक समूहों ने हथियार छोड़े।
 सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह परिवर्तन केवल पुलिसिया दबाव का परिणाम नहीं, बल्कि विकास और संवाद की नीति के समानांतर चलने से संभव हुआ है। सड़कें, मोबाइल नेटवर्क, स्कूल, अस्पताल और आजीविका मिशन अब उन इलाकों तक पहुँचने लगे हैं जो कभी मानचित्र पर सिर्फ प्रशासनिक बिंदु भर थे।
सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह परिवर्तन केवल पुलिसिया दबाव का परिणाम नहीं, बल्कि विकास और संवाद की नीति के समानांतर चलने से संभव हुआ है। सड़कें, मोबाइल नेटवर्क, स्कूल, अस्पताल और आजीविका मिशन अब उन इलाकों तक पहुँचने लगे हैं जो कभी मानचित्र पर सिर्फ प्रशासनिक बिंदु भर थे।
राज्य नीतियाँ और पुनर्वास की दिशा
सरकारों ने यह समझ लिया है कि केवल सैन्य बल से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जहाँ कभी जवाब में गोलियाँ थीं, अब वहाँ पुनर्वास केंद्र, शिक्षा के अवसर और रोजगार योजनाएँ हैं। छत्तीसगढ़ की “नक्सल पुनर्वास नीति 2023” के तहत आत्मसमर्पण करने वालों को पाँच लाख रुपये तक की सहायता, सुरक्षित आवास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और परिवार पुनर्स्थापन की सुविधा दी जा रही है। झारखंड, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ने भी इसी दिशा में नीतियाँ बनाईं हैं, जिनमें कानूनी संरक्षण के साथ स्वरोजगार और शिक्षा की गारंटी दी जाती है।
इन योजनाओं का मकसद केवल नक्सलियों को मुख्यधारा में लाना नहीं, बल्कि उन्हें समाज में गरिमामय जीवन देना है। यह प्रक्रिया तभी सफल होगी जब समाज स्वयं उन्हें स्वीकार करे और पुनर्वास को केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक साझेदारी के रूप में देखे।
व्यक्तिगत बदलाव की कहानियाँ
दंतेवाड़ा के अबूझमाड़ के एक पूर्व बटालियन कमांडर बताते हैं कि उन्होंने आत्मसमर्पण तब किया जब परिवार वर्षों तक भय में जीता रहा। आज वे एक सरकारी विद्यालय में सुरक्षा कर्मी हैं और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। झारखंड के गढ़वा जिले में आत्मसमर्पण करने वाली एक महिला, जो कभी नक्सल दस्ते की सदस्य थी, अब स्वरोजगार योजना के तहत बांस के उत्पाद बनाती है और स्थानीय मेलों में उन्हें बेचती है।
ये कहानियाँ बताती हैं कि आत्मसमर्पण केवल हिंसा का अंत नहीं, बल्कि आत्मबोध और पुनर्निर्माण की यात्रा की शुरुआत है।
चुनौतियाँ और अविश्वास की परतें
हालाँकि आत्मसमर्पण की बढ़ती घटनाएँ आशा जगाती हैं, लेकिन रास्ता सरल नहीं है। कई आत्मसमर्पित नक्सलियों को सुरक्षा खतरा, सामाजिक भेदभाव और वादे पूरे न होने की समस्याओं से जूझना पड़ता है। कुछ नक्सली गुट उन्हें ‘विश्वासघाती’ कहकर निशाना बनाते हैं। इसलिए सरकार को पुनर्वास नीतियों को सिर्फ कागज़ी दस्तावेज़ न रखकर, ज़मीन पर प्रभावी ढंग से लागू करना होगा।
सुरक्षा के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक सहायता और सामाजिक पुनर्संवाद को भी नीति का हिस्सा बनाना आवश्यक है। जब तक समाज और शासन दोनों मिलकर इन लोगों के भीतर विश्वास की भावना नहीं जगा पाते, तब तक यह परिवर्तन अधूरा रहेगा।
विकास और शिक्षा : स्थायी शांति की कुंजी
शिक्षा और रोजगार की पहुँच ने नक्सल आंदोलन की जड़ों को कमजोर किया है। “आदिवासी युवाओं के कौशल विकास मिशन” और “राजीव युवा शक्ति योजना” जैसे कार्यक्रम युवाओं के लिए नए अवसर लेकर आए हैं। जब राज्य बुनियादी सुविधाएँ और न्याय सुनिश्चित करता है, तो बंदूक का आकर्षण स्वयं मिटने लगता है।
युवा पीढ़ी अब जंगलों की अंधेरी गलियों में नहीं, बल्कि विद्यालयों और प्रशिक्षण केंद्रों में भविष्य खोज रही है। यह परिवर्तन बताता है कि हिंसा नहीं, अवसर ही परिवर्तन का वास्तविक मार्ग है।
आत्मसमर्पण से आगे : सामाजिक न्याय की आवश्यकता
यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त होने की कगार पर है। आंदोलन की जड़ें भूमि अधिकारों, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, असमानता और उपेक्षा में हैं। यदि इन मूल कारणों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो असंतोष किसी नए रूप में फिर से जन्म ले सकता है।
शांति तभी स्थायी होगी जब उसमें न्याय, समानता और पारदर्शिता की नींव होगी। केवल सुरक्षा दृष्टिकोण नहीं, बल्कि न्यायसंगत विकास ही स्थायित्व ला सकता है।
एक नए अध्याय की ओर
भारत के जंगल अब धीरे-धीरे बंदूक की गूँज से मुक्त होकर संवाद और विकास की आवाज़ सुनने लगे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की कहानियाँ इस बात की साक्षी हैं कि मानव मन अंततः शांति और सम्मान की ओर लौटना चाहता है। यह प्रक्रिया केवल शासन की सफलता नहीं, बल्कि समाज की सहिष्णुता और परिवर्तन की क्षमता का भी प्रमाण है।
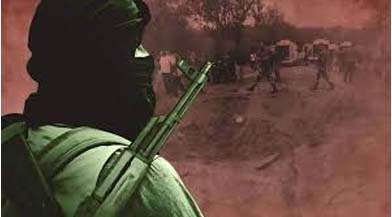 नक्सलियों का आत्मसमर्पण भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का वह पड़ाव है, जहाँ हिंसा अपने ही उद्देश्य से परास्त हो रही है। यदि यह रफ्तार न्याय, संवाद और विकास की संवेदना के साथ आगे बढ़ी, तो वह दिन दूर नहीं जब “रेड ज़ोन” सिर्फ इतिहास की एक पंक्ति रह जाएगा — और देश के इन अंचलों में फिर से जीवन, उम्मीद और विश्वास का सूरज उगेगा।
नक्सलियों का आत्मसमर्पण भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का वह पड़ाव है, जहाँ हिंसा अपने ही उद्देश्य से परास्त हो रही है। यदि यह रफ्तार न्याय, संवाद और विकास की संवेदना के साथ आगे बढ़ी, तो वह दिन दूर नहीं जब “रेड ज़ोन” सिर्फ इतिहास की एक पंक्ति रह जाएगा — और देश के इन अंचलों में फिर से जीवन, उम्मीद और विश्वास का सूरज उगेगा।






